essay about teachers day in hindi ! शिक्षक दिवस पर निबंध ! teachers day 2021
शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं ।
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान आदर्श, प्रशासक, शिक्षक, दार्शनिक एवं राजनितिज्ञ थे। इन्हीं योग्यताओं के आधार पर वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा भारत के उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। वे एक मनीषी, शिक्षक और सच्चे शिक्षाविद् थे। यही कारण है कि उनके नाम पर 5 सितम्बर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
essay about teachers day in hindi ! Shikshak diwas par nibandh in hindi
Content-
- शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं ।
- शिक्षक दिवस पर शिक्षा संस्थाओं में आयोजन-
- शिक्षा एवं शिक्षा का महत्व
- शिक्षक एवं शिक्षक का महत्व, गुरू का शाब्दिक अर्थ
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन बायोग्राफी
- शिक्षक की भूमिका
- शिक्षक के गुण
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा, दर्शन , विचार
- Sarvepalli Radhakrishnan quotes
शिक्षक दिवस पर शिक्षा संस्थाओं में आयोजन-
राष्ट्रपति डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन (5 सितम्बर) को प्रतिवर्ष 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल में छात्र शिक्षक बनकर अपने जूनियर छात्रो को पढ़ाते है एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इस उपलब्ध पर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पूजा की जाती हैं। शिक्षकों द्वारा आर्शीवचन प्रदान कीया जाता हैं। शिक्षक दिवस में शिक्षक आज छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए पथ प्रर्दशन करते हैं।
शिक्षा एवं शिक्षा का महत्व (शिक्षक दिवस का महत्व )
किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानव है। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को विकास के सर्वौतम अवसर मिले तथा वे उनका लाभ उठाने के लिए समर्थ हो । वस्तुतः मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा प्रणाली ही है ।
शिक्षा ही व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है । शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को सभ्य व सुसंस्कृत बनाकर उसे समाज व राष्ट्र का एक उपयोगी नागरिक बनाया जाता है । शिक्षा की यह प्रक्रिया जन्म से प्रारम्भ होकर मृत्यु पर्यन्त लगातार किसी न किसी रूप में एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है । प्रारम्भ में माता-पिता परिवार के अन्य सदस्यों तथा पड़ोसियों आदि से अनौपचारिक ढग से शिक्षा प्राप्त करता है ।पांच से छः वर्ष की आयु होने पर बालक की शिक्षा की व्यवस्था औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में सुनियोजित ढंग से प्रारम्भ हो जाती है । विद्यालय में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ बालक घर, समाज, धर्म जनसंचार आदि अनेक औपचारिकतर माध्यमों से भी कुछ न कुछ सीखता रहता है । औपचारिक शिक्षा के उपरान्त भी सीखने सिखाने का क्रम किसी न किसी रूप में अनवरत चलता रहता है ।
शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है । शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है जीवन को आनन्दमय बनाता है तथा जनकल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है।
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प खिल जाता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा रूपी प्रकाश पाकर मानव जीवन कमल के पुष्प के समान खिल उठता है तथा उनकी कीर्ति चारों दिशाओ में फैल जाती है । इसके विपरीत शिक्षा रूपी प्रकाश के अभाव में व्यक्ति अज्ञानता, दरिद्रता व कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है ।
 |
| happy teachers day image wishes |
वास्तव में शिक्षा एक ओर जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उनकी व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है वही दूसरी ओर वह उसे समाज का एक महत्वपूर्ण व उत्तरदायी स्वस्थ तथा राष्ट्र का एक सुयोग्य, कर्तव्यनिष्ठ व सजग नागरिक भी बनाती है । शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी भावी पीढ़ी को उच्च आर्दशों अभीष्ट आशाओं उत्कृष्ठ आकांक्षाओं, सनातन मूल्यों, सतत् विश्वासों तथा प्राचीन परम्पराआं से युक्त अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हस्तानान्तरित करता रहता है ।
शिक्षा बालक के ह्दय में, देश प्रेम, बलिदान व निहित स्वार्थों के त्याग की भावना को प्रज्ज्वलित करती है । उचित ढंग से शिक्षित नागरिकों के अनुकरणीय कार्यों के फलस्वरूप ही समाज एवं राष्ट्र निरन्तर उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होतें है ।स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका अदा करती है ।निःसंदेह शिक्षा सतत् रूप से चलने वाली एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जो मानव को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने में सक्षम बनाती है एवं राष्ट्र के विकास में सहायता प्रदान करती है ।शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाकर ही राष्ट्र की प्रगति तथा विकास की निरन्तरता को जारी रखा जा सकता है।
शिक्षा को सदैव से ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सदैव ही शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से एक सम्मान जनक स्थान दिया जाता रहा हैं!
स्वामी विवेकानंद के वाक्य
'' Education is manifestation of perfection already present in man ''
शिक्षक एवं शिक्षक का महत्व। गुरू का शाब्दिक अर्थ
शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, प्राचीन काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास में उसका विशेष योगदान रहा है । अध्यापकों में शिक्षार्थियों की आस्था होती है । विद्यार्थिो के व्यवहार परिमार्जन में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है । शिक्षक को भारतीय परम्पराओं में ‘गुरू’ शब्द से सम्बोधित किया जाता है, गुरू शब्द में ‘गु’ अंधकार का प्रतीक है तथा ‘रू’ ज्ञान के लिए होता है, इस प्रकार गुरू का शाब्दिक अर्थ अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला । गुरू अपने ज्ञान से शिष्य को पुष्पित व पल्लवित करता है चूकि अध्यापक कालजयी होता है वह न्यायधीश की तरह निष्पक्ष, संयासी की तरह निर्भीक, चिकित्सक की तरह सेवक, सेनापति की तरह साहसी, साधू की तरह उदार, माता की तरह दानी तथा पिता की तरह शुभेच्छु होता है । इस तरह अध्यापक का व्यक्तित्व पारदर्शी तथा स्पष्ट होना चाहिए । उसे झूठ, सच, न्याय, अन्याय, उचित-अनुचित में समझौता न करते हुए नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए।
अध्यापक का अमूल्य धन उसका स्वाभिमान होता है । उसे संयम, चिन्तन, सम्यक् दृष्टिकोण स्नेह तथा उदारता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए । शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगो में अध्यापक छात्र व पाठ्यवस्तु मे अध्यापक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयाग्य छात्रगण अच्छी पाठ्यवस्तु होते हुए भी वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार से अच्छी से अच्छी पाठ्यवस्तु भी निपुण अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करतें हैं अच्छे अध्यापक छात्रों को वांछित व्यवहार परिवर्त न में सहायता प्रदान करते हैं, तथा सर्वांगीण विकास के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं ।
शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों न हो उनमें अध्यापक की भूमिका सर्वापरि होती है । अध्यापक, शिक्षा प्रणाली का केन्द्र होता है तथा समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चहु ओर विचरण करती हैं । अध्यापक को शिक्षा व्यवस्था का प्राण कहना भी अनुचित नहीं होगा, क्योकि शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था को जीवन्त बनाता है । हमारा वर्तमान समाज राष्ट्रीय परिवर्तन व विकास के एक नाजुक परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है । शिक्षक ही देश के भावी नागरिकों अर्थात छात्र-छात्राओं के वास्तविक सम्पर्क में आता है तथा उन्हें अपने आचार-विचार तथा ज्ञान के अवबोध से प्रभावित करता है । शिक्षकों के ऊपर ही राष्ट्र के भावी निर्माताओं को तैयार करने का दायित्व होता है । किसी भी राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का सूत्रधार अध्यापक ही होता है ।
समाज की आवश्यकतों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, आदर्शों, मूल्यों आदि को वास्तविक रूप देने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को वहन करनी होती है । वास्तव में अध्यापकगण अपने प्रयासों से भावी समाज की संरचना करते हैं । इसलिए आजकल शिक्षको को सामाजिक अभियन्ता के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के कार्य में शिक्षकों की भूमिका तथा योगदान को देखत हुए अध्यापक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है ।
प्राचीन काल से ही समाज में भावी नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा अन्य सभी प्रकार के विकास करने का कार्य शिक्षकों को सौपनें की परम्परा रही है ।शिक्षक का कार्य ज्ञान व संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तानान्तरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। राष्ट्रीय आवश्कताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए सृजनशील नेतृत्व को विकसित करना समानता, स्वतंत्रता व न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान भी शिक्षक समुदाय का उत्तरदायित्व है ।
- डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के अनुसार ‘‘समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बौद्धिक परम्पराओं व तकनीकी का कौशलों के हस्तान्तरण के साधन के रूप में तथा सभ्यता की ज्योति को प्रज्जवलित रखने में सहायता प्रदान करता है ।’’
- पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अध्यापकों की भूमिका के विषय में कहा था कि ‘‘अध्यापकों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों व संस्कृति जो उसके साधन हैं, को द्वारा अपने छात्रों को उच्च मूल्यों को हस्तान्तरण में सहायता करनी चाहिए।''
- अध्यापकों को अंकुर को पूर्ण रूप से खिलने में सहायता प्रदान करनी चाहिए न की अपनी पूर्ति के लिए कृत्रिम पुष्प तैयार करने चाहिए । नैतिक दृष्टि स्वायत्त व्यक्तित्व personality development का विकास करना ही अध्यापकों के परीश्रम का लक्ष्य व परिणाम होना चाहिए ।’’
- बालकृष्ण जोशी का परामर्श है -‘‘शिक्षक को अपने को केवल श्रमजीवन नहीं समझना चाहिए जिसका कार्य 10 बजे आरम्भ होता है और 4 बजे समाप्त होता है जब वह अपने पैरों की धूल झाड़कर जीविका प्रदान करने वाले विद्यालय रूपी फैक्ट्री से बाहर जा सकता है।’’
शिक्षक की भूमिका
भारत में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण संसार में शिक्षण को एक श्रेष्ठ व्यवसाय माना गया है । मानव इतिहास की श्रेष्ठतम विभूतियों ने इस व्यवसाय को अपनाया है । समस्त युगों के समस्त धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों ने इस व्यवसाय को अंगीकार करको इसको गौरव में अभिवृद्धि की है । बुद्ध इसा मसीह, महात्मा गांधी, सुकरात, मुहम्मद साहब कन्फ्यूसियस ये सभी सच्चे अर्थ में मानव जाति के शिक्षक थे । उन्होंने अपने समाज के सामान्य व्यक्तियों द्वारा जीवन में स्वीकार किये जाने वाले मानदण्डों का साहस और इमानदारी से विश्लेषण किया और उनको उच्चतर जीवन के आदर्श एवं कल्पना से परिचित कराया ।
शिक्षक का भूमिका-
- शिक्षक को विषय का पर्याप्त ज्ञान एवं आत्मविश्वास होना चाहिए ।
- शिक्षण विधि में विविधता तथा ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करना चाहिए ।
- भाषा में प्रवाह होना चाहिए ।
- अधिगमकर्ताओं के प्रति ज्ञान संवेदना होनी चाहिए ।
- शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया तथा शिक्षण अभ्यास की क्षमता का विकास करना चाहिए ।
- शिक्षक को शिक्षण अधिगम उपागम में सुधार करना चाहिए ।
- शिक्षक प्रभावशाली अधिगम वातावरण का सृजन एवं निरन्तरता बनाये रखने की योग्यता का विकास करना चाहिए ।
- शिक्षक को पाठ्यक्रम एवं उसके उद्देश्यों की समझ होनी चाहिए ।
- शिक्षक को सामान्य शिष्टाचार एवं शिक्षण के प्रति समर्पित होना चाहिए ।
- शिक्षक में प्रभावशाली सम्प्रेषण क्षमता का विकास होना चाहिए ।
- शिक्षक को सदाचार नैतिकता तथा व्यक्तिगत अनुशासन का विकास करना चाहिए ।
राष्ट्र निर्माण में योग्य एवं कुशल शिक्षकों के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता है । क्योंकि बच्चों की उपलब्धि एवं गुणवत्ता योग्य एवं संवेदनशील शिक्षकों पर निर्भर करती है । शिक्षक किसी भी दशा में विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता है । इसके साथ ही उसे निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करना, विद्यार्थियो का मूल्यांकन करना, अभिभावकों का सम्मेलन करना तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, विद्यालय प्रबन्ध समिति संगठन करना इत्यादि दायित्वों का निर्वहन भी करना होता है ।
शिक्षक के गुण
शिक्षकों के ज्ञान, समझ, कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण, आदत, मूल्य एवं क्षमताओं से युक्त ऐसे शिक्षक की संकल्पना की गयी है जिसमें निम्नलिखित गुण विद्यमान हों-
- बच्चों की देखभाल और उनके साथ प्रेम, बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सन्दर्भ को समझना ।
- बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को प्रति संवेदना विकसित करना तथा बच्चों के साथ समान व्यवहार करना ।
- बच्चों को ज्ञान के निष्क्रिय उपभोक्ता होने पर बच्चों के प्राकृतिक क्षमता के उपयोग द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माता समझना ।
- रटन्त अधिगम को हतोत्साहित करना, अधिगम को आनन्दायक सहगामी एवं अर्थ पूर्ण गतिविधि के रूप में निर्मि त करना ।
- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तको को आलोचनात्मक परीक्षण करना पाठ्यक्रम के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना ।
- ज्ञान को पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान करने तथा बिना तर्क के स्वीकार करने को हतोत्साहित करना ।
- अधिगम केन्द्रित, गतिविधि आधारित, सहगामी अधिगम अनुभव जैसे- खेल, परियोजनाएं, परिचर्चा , वाद-विवाद, अवलोकन भ्रमण एवं स्वयं के अभ्यास से अधिगम को संगामी करना ।
- शैक्षणिक अधिगम को सामाजिक एवं अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत वास्तविकताओं तथा कक्षा में विभिन्नताओं को सम्मान प्रदान करना ।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार । Sarvepalli Radhakrishnan quotes
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा, दर्शन , विचार
डॉ, राधाकृष्णन ने अपने शिक्षा दर्शन में शिक्षक की अहम भूमिका को स्वीकार किया है।है। वे कहते हैं कि सबसे महान शिक्षक वे हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीवन्त रखा हैं। शिक्षक देश के सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य रूप से विद्यार्थी को प्रदान करें। शिक्षकों के कार्यों तथा व्यक्तित्व का अमिट छाप विद्यार्थियों के चरित्र पर अंकित होता हैं। उन्हें ज्ञान पिपासु होना चाहिए। डॉ राधाकृष्णन स्वयं एक महान शिक्षक रहें।
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वाक्य । Sarvepalli Radhakrishnan quotes -
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा, दर्शन , विचार । essay about teachers day in hindi
the function of the teachers is of vital importance. he must be a committed man. commited to faith in the future of humanity in the future of the country and world.
We recognise that the profession of teaching is that which contributes to the trans mission of our intellectual heritage and our technical skills and to the training of our people for the development of the country. the function of the teacher is to assist the growth by stimulation and guidance. the growth is advanced by the acquision of knowledge and skills.
A true educator should understand the psychological make up the svabhav of the pupil and adapt his teaching to the mind of the pupil. the teachers should discover the tendencies and weakness of the indivial pupils, encourage their desirable aptitudes and cure the weakness to which they are inclined.
- The importance of the teacher and his responsibility the success of the educational process depends so much on the characters and ability of the teacher the aims and objective of teaching briefly stated they are-
- Transmission the intellectual and ethical heritage of humanity to the young.
- Enrichment of this heritage and extension of the boundaries of knowledge.
- Development of personity
The primary responsibility of the teacher is to arouse the interest of the pupil in the field of study. he was not merely to convey factual information and the principles. he has to stimulate the spirit of equity and of critism.
- The teacher ids also the bearer of the traditions and ideal which constitutes the ethos of a society. the right kind of teacher is one who possesses a vivid awareness of his mission, he not only loves his subject, he loves also those whom he teaches, his success will be measured not in terms of percentage of passes alone, even by the quantity of original contribution to knowledge, important as they are, but equally through quality of life and character of men and women whom he has taught.
डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षकों को परम्पराओं तथा मूल्यों का संवाहक मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षक में ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए। उनके ज्ञान का मूल्यांकन पास करना या प्रतिशत बढ़ाने पर नहीं होना चाहिए। बल्कि छात्रों के उत्तम चरित्र से हो चाहिए।

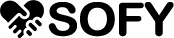




0 Comments